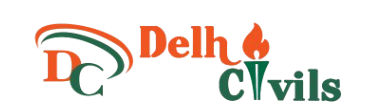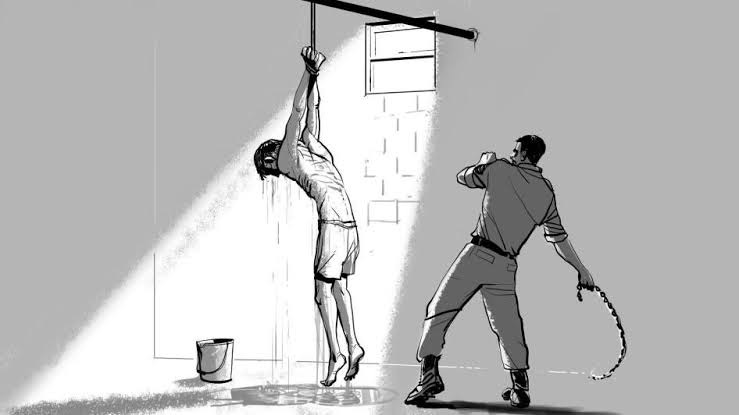हाल ही में लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से आगामी छह माह के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। यह घटनाक्रम राज्य में लगभग दो वर्षों से चल रहे जातीय संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुआ, जो कि घाटी में रहने वाले मैती समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति कूकी-जो समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। यह संघर्ष मुख्यतः मैती समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (ST) दर्जे की माँग और कूकी समुदाय द्वारा उसके विरोध से उत्पन्न हुआ था, जिसमें कूकी समुदाय को रोजगार और आरक्षण जैसे विशेषाधिकारों के नुकसान का भय था।
भारतीय संविधान के भाग XVIII के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधान जर्मन संविधान से प्रेरित हैं, जो भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ प्रदान करते हैं। आपातकाल की तीन श्रेणियाँ हैं — राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352), राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356), और वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)। राष्ट्रपति शासन, जिसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत तब लागू होता है जब किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाती है। इसकी सिफारिश राज्यपाल की रिपोर्ट या राष्ट्रपति की स्वयं की संतुष्टि के आधार पर की जा सकती है।
इस स्थिति में राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ केंद्र सरकार को हस्तांतरित हो जाती हैं, जबकि विधानमंडल निलंबित या भंग किया जा सकता है। उच्च न्यायालय का कार्य इस दौरान अप्रभावित रहता है। अनुच्छेद 365 यह भी प्रावधान करता है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों की अवहेलना करता है, तो राष्ट्रपति संवैधानिक संकट घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो माह के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना होता है और यह छह माह के लिए प्रभावी होता है। इसकी अवधि अधिकतम तीन वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है, बशर्ते राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं है।
राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में महत्वपूर्ण अंतर है। राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) पूरे देश या किसी भाग में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू होता है, जबकि राष्ट्रपति शासन केवल उस राज्य पर लागू होता है जहाँ संवैधानिक तंत्र विफल हुआ हो। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, विशेषकर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताएँ, जबकि राष्ट्रपति शासन के दौरान मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं।
राष्ट्रपति शासन की संवैधानिक वैधता और सीमा को सुप्रीम कोर्ट ने एस. आर. बुम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में स्पष्ट किया, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद राज्य सरकार को पद छोड़ना होता है क्योंकि एक साथ दो सरकारें नहीं चल सकतीं।
इतिहास में अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग लगभग 134 बार हो चुका है, जिसमें सबसे पहली बार 1951 में पंजाब में और सबसे अधिक बार मणिपुर और उत्तर प्रदेश में (10 बार) लागू हुआ है। मणिपुर का वर्तमान मामला इसे 11वीं बार बना देता है। जम्मू-कश्मीर ने राष्ट्रपति शासन के तहत सबसे लंबी अवधि (12 वर्षों से अधिक) देखी है, इसके बाद पंजाब और पुडुचेरी का स्थान आता है।
इस प्रकार, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन का यह विस्तार केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं बल्कि भारत के संघीय ढांचे और राज्यों की स्वायत्तता के बीच संतुलन की परीक्षा भी है।
🧾 Prelims के लिए संभावित प्रश्न (UPSC/PCS):
Q1. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?
A. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य के उच्च न्यायालय का कार्य बाधित होता है।
B. अनुच्छेद 356 के तहत लगाया गया राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा से परे है।
C. राष्ट्रपति शासन अधिकतम 5 वर्षों तक चल सकता है।
D. राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ केंद्र को स्थानांतरित हो जाती हैं।
उत्तर: ✅ D
Q2. S.R. बुम्मई केस (1994) किससे संबंधित है?
A. मौलिक अधिकारों की समीक्षा
B. वित्तीय आपातकाल की प्रक्रिया
C. राष्ट्रपति शासन की न्यायिक सीमा
D. अनुच्छेद 370 की व्याख्या
उत्तर: ✅ C
Q3. राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है?
A. 1 वर्ष
B. 3 वर्ष
C. 5 वर्ष
D. 6 माह
उत्तर: ✅ B